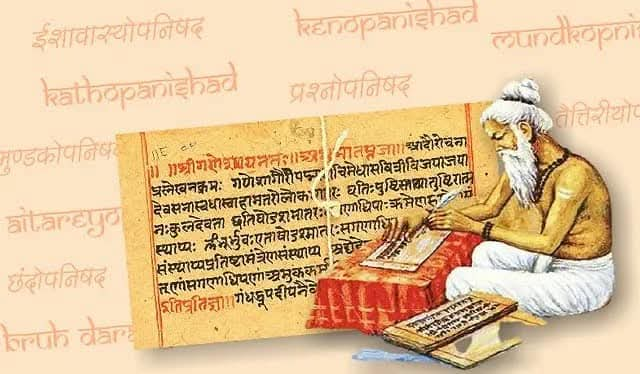प्रशांत पोळ
अनेक स्थानों पर मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा पर बोलने हेतु आमंत्रित किया जाता हैं। उन सभी स्थानों पर, मैं प्रोफेसर अंगस मेडिसन का उल्लेख अवश्य करता हूं। इस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनेक पुस्तकें लिखी। इन पुस्तकों में अनेक संदर्भ देकर, आंकड़े प्रस्तुत कर, उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया, कि किसी जमाने में भारत यह विश्व का सबसे वैभवशाली, सबसे संपन्न राष्ट्र था। विश्व के व्यापार का एक तिहाई व्यापार मात्र भारत करता था, और विश्व की 30% से भी ज्यादा संपत्ति भारत के पास थी।
विदेशी आक्रांता भारत में आने से पहले हम कितने संपन्न और समृद्ध थे, इसका यह सशक्त प्रमाण हैं।
यह सब पढ़ते समय, एक प्रश्न मन में उठता हैं। हम विश्व में सबसे ज्यादा व्यापार करते थे। हमारे जहाज लैटिन (दक्षिण) अमेरिका तक जाते थे। हमारी वस्तुओं की गुणवत्ता भी अत्यंत उच्च दर्जे की थी, इसलिए हमारी वस्तुओं की विश्व में अच्छी खासी मांग थी। हमारे यहां जो वस्त्र तैयार होते थे, उन्हें खरीदने के लिए अलग-अलग देशों के राजा – महाराजाओं में होड़ लगती थी। मानवी कुशलता, मानवी कौशल हैरान होगा, ऐसे भव्य मंदिर, महल, राजप्रासाद हमने बनाएं। विश्व का सबसे बड़ा प्रार्थना स्थल, अंगकोर वाट जैसा सुंदर मंदिर समूह, हमने खड़ा किया। अनेक धातु खोज निकाले। जल व्यवस्थापन में महारत हासिल की। तकनीकी में हम समय से बहुत आगे बढ़ गए।
यह इतना सब, हम ‘मैनेज’ कैसे करते होंगे..?
अपने पूर्वजों ने प्रबंधन (व्यवस्थापन – मैनेजमेंट) की कोई अधिकृत शिक्षा ली थी क्या? या पहले तक्षशिला, और बाद में नालंदा, उड्डयंतपुर, विक्रमशिला, वल्लभी, सुलोटगी जैसे विश्वविद्यालयों में, प्रबंधन (व्यवस्थापन) यह विषय पढ़ाया जाता था ? ऐसे अनेक प्रश्न। अत्यंत उत्कृष्ट, उच्च गुणवत्ता का सटीक काम हमारी अनेक पीढ़ियों ने, उस कालखंड में किया, यह तो निश्चित हैं। फिर, ये कैसे संभव हुआ? आज के जमाने में, बिजनेस स्कूल या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढकर, एम बी ए जैसी डिग्रियां लेकर आए युवक – युवतियां ही प्रबंधन का सब काम देख सकते हैं, ऐसा उद्योग जगत का विश्वास हैं। वैसा ही, उस समय भी होता था क्या?
अर्थात एक निश्चित है, प्राचीन शिक्षा पद्धति के बारे में जो जानकारी मिली हैं, उसके अनुसार, उस समय के पाठ्यक्रम में प्रबंधन / व्यवस्थापन जैसे विषय नहीं थे। व्यवस्थापन का अलग से विभाग नहीं था, और ना ही व्यवस्थापन पढ़ने वाली संस्थाएं थी। इसके बावजूद भी, हमारे पूर्वज, पूरे विश्व में भव्य – दिव्य साकार कर रहे थे। उस समय के सबसे बड़े जहाज बनाकर दुनिया के देशों को बेच रहे थे। नए-नए शोध लगा रहे थे, और साफ सुथरा व्यापार भी कर रहे थे।
हमारे इन पूर्वजों ने यह सब कैसा किया होगा, यह समझना हैं, तो आज के ‘मैनेजमेंट’ का चश्मा उतार कर, पूरी प्रक्रिया को समझना होगा।
हमारे उस स्वर्णिम कालखंड में, प्रबंधन यह विषय सीधे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। इसलिए प्रबंधन पढ़ाया नहीं जाता था। प्रबंधन के सारे तत्व, अप्रत्यक्ष रूप से, किंतु अत्यंत प्रभावी तरीके से, विद्यार्थियों तक पहुंचते थे।
इस प्रक्रिया में ‘उपनिषद’ यह महत्व का माध्यम था। लगभग 4000 से 6000 वर्ष पूर्व, अपने पूर्वज ऋषि-मुनियों ने, 108 उपनिषद लिखे। इनमें से 10 प्रमुखता से पढ़े जाते थे / पढ़ाए जाते थे। आज के समय में हम गीता, उपनिषद, भागवत जैसे ग्रंथ, यानी सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास करने के लिए बने धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐसा मानते, समझते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। तब धर्म का अर्थ भी अलग था। कर्मकांड कम थे। एक अच्छी, उच्च आदर्शो से प्रेरित उदात्त जीवन शैली यानी धर्म, ऐसा माना जाता था। लड़के – लड़कियां पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाते थे। वहीं पर उनका उपनिषदों से परिचय होता था। उपनिषद यानी कठिन और जटिल संकल्पनाओं के उबाऊ (बोअरिंग) ग्रंथ नहीं थे। वह तो छोटी-छोटी किस्से – कहानियों से भरी पुस्तकें थी। किंतु इन पुस्तकों में संदेश छुपे रहते थे। यह संदेश ही विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा थी। जीवन जीने की कला थी।
आधुनिक मैनेजमेंट की हवा मुख्यतः अमेरिका से बहना प्रारंभ हुई। अमेरिका यह पूर्णतः व्यापारिक देश। उस देश की जो मूल सभ्यता थी, वह वहां के रेड इंडियन्स (नेटिव्स) की थी। उसे तो यूरोप से आए हुए लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया। इसलिए यूरोप से आकर यहां पर बसे लोगों का मूल मंत्र ‘पैसा’ होगा, यह स्वाभाविक ही था। इसलिए, अमेरिका में मैनेजमेंट में, जिस किसी को थोड़ी बहुत सफलता मिलती हैं, अमेरिकन्स उसके पीछे भेड़ – बकरियों जैसे दौड़ते हैं।
साठ – सत्तर के दशक में अमेरिका में डेल कार्नेगी के प्रबंधन शैली का बोलबाला था। उसकी ‘हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इनफ्लुएंस पीपल’ जैसी पुस्तक, लाखों की संख्या में बिक रही थी। फिर TA ट्रांजैक्शन एनालिसिस आया। ‘आई एम ओके यू आर ओके’ की संकल्पना आई। अभी कुछ वर्ष पहले, भारतीय मूल के शिव खेड़ा की हवा बह रही थी। ये सारे लोग और उनकी प्रबंधन शैली, उन-उन दिनों जबरदस्त लोकप्रिय रही। इन सब लोगों ने मानवी स्वभाव की बारीकियों पर और उसके द्वारा उत्पादनक्षमता बढ़ाने पर जोर दिया।
मजेदार बात यह, कि ये सारी बातें, अलग पद्धति से, हमारे यहां कुछ हजार वर्ष पहले, अपने ऋषि मुनियों ने, उपनिषद, गीता आदी ग्रंथों मे विस्तार से लिख रखी हैं।
इन सब उपनिषदों का या भगवद् गीता की सीख का आधार, नैतिकता, सदाचार और प्रमाणिकता था। यह सारे मात्र आदर्श तत्व नहीं थे, कि ‘जो आदर्श तो हैं, किंतु व्यवहार में उतारना संभव नहीं हैं’। नैतिकता, सदाचार, प्रमाणिकता यह सारे जीवनमूल्य थे। व्यापार समवेत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू थे। इसलिए व्यापार में और व्यवहार में छल – कपट को स्थान नहीं था।
मंडुक्य उपनिषद में शांति मंत्र है
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः।
भद्रं पश्येमाक्षभि: यजत्राः।।
अर्थात, ‘जो मंगलकारी हैं, कल्याणकारी हैं, वही हम सुन सके। हमारे कान, हमारा मन, सदैव निर्मल रहे’। इस श्लोक में ‘यजत्रा’ शब्द का प्रयोग किया गया हैं। यजत्रा का अर्थ, यज्ञ करने वाले लोग। किंतु उपनिषदकार बताते हैं, यज्ञकुंड में अग्नि प्रज्वलित करके जो करते हैं, वही मात्र यज्ञ नहीं हैं। यज्ञ बुद्धि का, यज्ञ ज्ञान का, यज्ञ कर्मशिलता का होना चाहिए। हमें समझ आने के बाद, हम समाज कल्याण के लिए जो करते हैं वह है यज्ञ..!
कितना स्पष्ट समझाया है !
मुंडकोपनिषद में एक श्लोक हैं –
सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः I
क्रमंत्यृषयो ह्याप्तकामो यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् II
अर्थात, सदैव सत्य की ही विजय होती है। मिथ्या या असत्य कभी भी जीत नहीं सकते। हमने 26 जनवरी 1950 को इस श्लोक के ‘सत्यमेव जयते’ को अपने देश का घोषवाक्य या आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया हैं।
नारायण उपनिषद के चौदहवें मयूरव में एक श्लोक है –
धर्म इति धर्मेण सर्वमिदं परिगृहीतम् I
धर्मांन्नातिदुशाश्चरं तस्माध्दर्मे रमन्ते II 6II
इसमें बताया हैं, स्वधर्म का आचरण यह उत्तम साधन हैं। सदाचार, सन्निती, प्रमाणिकता, विश्वसनीयता यह सब हमारे धर्म के अंग हैं। शास्त्र पर श्रद्धा, यह धर्म का प्राण हैं।
ये सब बातें, गुरुकुल के माध्यम से, विद्यालयों और विद्यापीठों से, घर के संस्कारों से, नीचे तक रिसते जाती थी। इसके कारण बाल्य काल से ही प्रमाणिकता, सदाचार आदि हमारे जीवनमूल्य हैं, यह बातें विद्यार्थियों के अंदर तक पहुंचती थी। इन सब का प्रभाव व्यापार में भी दिखता था, और इसीलिए विश्व के अनेक देशों के व्यापारी, राजा – महाराजा, अमीर – उमराव, भारतीयों पर और भारतीय माल पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। भारत का व्यापार, भारतीय वस्तुओं के गुणवत्ता के कारण तो बढा और फला-फुला ही, किंतु उसमें एक और बात थी – प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की..! आज के प्रबंधन की भाषा में, ‘एथिकल कोड आफ कंडक्ट’।
क्रमशः प्रशांत पोळ
(‘खजाने की शोधयात्रा’ इस पुस्तक के अंश। इस पुस्तक का विमोचन, शनिवार 26 जुलाई को माननीय उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दिल्ली मे होने जा रहा है।)